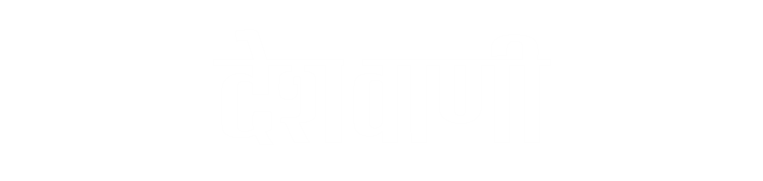राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों की समीक्षा की मांग की है। RSS का कहना है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़े गए थे और मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया था।
RSS की दलीलें-
RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये शब्द आपातकाल के उस दौर में जोड़े गए थे, जब लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। होसबोले ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा तो हुई, लेकिन इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
आपातकाल का जिक्र-
होसबोले ने 25 जून, 1975 को घोषित आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गयीं। साथ ही, न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया गया था।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय था और लाखों लोगों को इस वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर बर्बरता और अत्याचार हुए थे।
RSS Calls for Review of ‘Socialist’ and ‘Secular’ in Constitution, Citing Emergency-Era Insertion
The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has called for a review of the words ‘socialist’ and ‘secular’ in the Preamble to the Indian Constitution. The organization argues that these terms were inserted during the Emergency period and were not part of the original Constitution drafted by B.R. Ambedkar.
RSS’s Argument Against the Terms
Speaking at an event marking 50 years of the Emergency, Dattatreya Hosabale, the RSS General Secretary, stated that Babasaheb Ambedkar never used these words in the Constitution’s Preamble. He emphasized that these terms were added during the Emergency (1975-1977), a time when fundamental rights were suspended. Hosabale noted that while discussions on this issue occurred later, no efforts were made to remove the two words from the Preamble.
Recalling the Emergency
Hosabale recalled the period of the Emergency, which was declared on June 25, 1975, stating that thousands of people were imprisoned and tortured, and the freedom of the judiciary and media was curtailed.
Union Minister Nitin Gadkari also attended the event, describing the Emergency as a dark period in the country’s history, during which lakhs of people suffered. Gadkari asserted that there was widespread barbarism and atrocitiesduring that time.
संविधान में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को जोड़ने का इतिहास
भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ (secular) शब्द शामिल नहीं थे. इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था. यह संशोधन आपातकाल (1975-1977) के दौरान किया गया था, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं.
42वां संशोधन: एक महत्वपूर्ण बदलाव
42वें संविधान संशोधन को अक्सर ‘लघु संविधान’ (Mini-Constitution) भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे. इस संशोधन के माध्यम से, प्रस्तावना में ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ के स्थान पर ‘संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ कर दिया गया था. इसके साथ ही, ‘राष्ट्र की एकता’ को ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ में बदल दिया गया।
संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना और उसमें जोड़े गए शब्दों के महत्व पर क्या कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में प्रस्तावना की भूमिका और उसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है, खासकर ‘मूल संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) के संदर्भ में.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973)
यह भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है. इस ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है।
कोर्ट ने ‘मूल संरचना सिद्धांत’ का प्रतिपादन किया, जिसके तहत संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी मौलिक हैं कि उन्हें संसद द्वारा संशोधित या नष्ट नहीं किया जा सकता।
- प्रस्तावना का महत्व: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है. इससे पहले, बेरुबारी यूनियन केस (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामले ने इस स्थिति को बदल दिया।
- प्रस्तावना ‘मूल संरचना’ का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या प्रस्तावना में शामिल सभी तत्व मूल संरचना का हिस्सा हैं, लेकिन यह संकेत दिया कि प्रस्तावना में निहित कुछ प्रमुख सिद्धांत, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता, संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग हो सकते हैं।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले के फैसले को और पुख्ता किया और मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994)
यह एक और महत्वपूर्ण मामला था जिसने धर्मनिरपेक्षता (Secularism) की अवधारणा को मजबूत किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है. कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भारत की पहचान और एकता के लिए मौलिक है. इस फैसले ने ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने के महत्व को और भी रेखांकित किया.
सारांश में
सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि:
- प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
- प्रस्तावना में निहित कुछ प्रमुख सिद्धांत, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और इन्हें संसद द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता.
- इन निर्णयों ने संविधान की मौलिक पहचान को बनाए रखने और भविष्य में किसी भी संभावित मनमाने संशोधन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संविधान की प्रस्तावना में निहित अन्य महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है और इसमें कुछ और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो भारत के स्वरूप और उसके आदर्शों को परिभाषित करते हैं. आइए उन पर एक नज़र डालते हैं:
1. संप्रभु (Sovereign)
यह शब्द बताता है कि भारत एक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति वाला राष्ट्र है. इसका मतलब है कि भारत आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है. हम अपने फैसले खुद लेते हैं और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं हैं.
2. लोकतांत्रिक (Democratic)
इसका अर्थ है कि भारत में शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का है. लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं. यह शब्द चुनाव, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों को रेखांकित करता है.
3. गणराज्य (Republic)
यह शब्द इंगित करता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है. इसका मतलब है कि सर्वोच्च पद किसी विशेष परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी योग्य नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है.
4. न्याय (Justice)
प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है:
- सामाजिक न्याय: इसका अर्थ है समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा.
- आर्थिक न्याय: इसका मतलब है कि धन, आय और संपत्ति की असमानताओं को कम किया जाएगा और सभी को आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएंगे.
- राजनीतिक न्याय: इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार.
5. स्वतंत्रता (Liberty)
यह शब्द नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है. इसका मतलब है कि लोग अपनी राय व्यक्त करने, अपने विश्वासों को मानने और किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक कि वे कानून का उल्लंघन न करें या दूसरों के अधिकारों का हनन न करें.
6. समानता (Equality)
प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है. इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा. सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो.
7. बंधुत्व (Fraternity)
यह शब्द भाईचारे की भावना को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर रहें. इसका उद्देश्य व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है. यह शब्द एक समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देता है जहाँ सभी एक-दूसरे का सम्मान करें.
ये शब्द मिलकर भारतीय संविधान के मूल दर्शन और मूल्यों का निर्माण करते हैं, जो एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समावेशी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखते हैं.